छाया : द कैरेवान
• सारिका ठाकुर
किसी की परवरिश उसके व्यक्तित्व निर्माण में खाद-पानी की भूमिका निभाती है, जड़ों को मजबूत बनाती है लेकिन किसी भी बीज की प्रतिकृति (Replica) तैयार नहीं करती। दुनिया जैसा चाहती है, उसके उलट इंसान अपने लिए अपनी रूचि का क्षेत्र भी चुन सकता है और अपने परिवार का नाम रौशन कर सकता है। प्रो. अपर्णा वैदिक इस बात की जीती जागती मिसाल हैं। इतिहास विषय लेकर अकादमिक क्षेत्र में अपने शोध कार्यों से अपनी अलग पहचान बनाने वाली अपर्णा के पिता अपने समय के सुविख्यात पत्रकार थे, लेकिन उनकी ओर से ऐसा कोई दबाव नहीं था कि बेटी भी पत्रकार बने।
अपर्णा वैदिक का जन्म 22 सितम्बर 1975 को इंदौर में हुआ। उनके पिता स्व. डॉ वेदप्रताप वैदिक ख्याति प्राप्त पत्रकार और भारतीय भाषाओं के पक्षधर थे, हिन्दी को विश्व मंच पर स्थापित करने के मामले में वे दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी और राम मनोहर लोहिया की अगली कड़ी माने जाते हैं। वे कुशल राजनितिक विश्लेषक होने के साथ ही विदेश नीति की गहरी समझ रखते थे। उन्होंने अपने देश के साथ साथ विदेशों के कई शिक्षण संस्थानों में विजिटिंग प्रोफ़ेसर के तौर पर काम किया। अपर्णा जी की माँ डॉ. वेदवती, दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में प्रोफ़ेसर थीं।
अपर्णा जी के जन्म के समय देश में आपातकाल लग चुका था, जिसके कारण उनके पिता भूमिगत थे, इसलिए वेदवती जी इंदौर अपने सास-ससुर के पास आ गयी थीं। स्थिति सामान्य होने के बाद वे वापस दिल्ली चली आयीं, जहाँ आपातकाल से पहले उनका परिवार रहता था। अपर्णा जी के बड़े भाई सुपर्ण वैदिक उनसे मात्र एक साल बड़े हैं। दोनों ही बच्चों को घर में एक स्वस्थ माहौल मिला। माता-पिता के बीच प्रायः सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होती, जिसमें बच्चों को भी सुनने, समझने और शामिल होने की पूरी आजादी थी। अपर्णा जी के पिता और दादा वगैरह आर्य समाजी थे। दादाजी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के पक्षधर थे, इसीलिए उनकी सभी बेटियाँ यानि वेद प्रताप जी की बहनों ने उच्च शिक्षा हासिल की। हालांकि लड़कियों की आज़ादी को लेकर उनकी एक निश्चित राय ज़रुर थी। लड़कियों का जींस पहनना या टी शर्ट पर अंग्रेज़ी में कुछ लिखा होना उन्हें पसंद नहीं था। अपने दादाजी को ‘बाबाजी’ के नाम से पुकारने वाली अपर्णा जी उनके बारे में बताती हैं कि वे बहुत दबंग थे और घर में उन्हीं की चलती थी। जब वे दिल्ली में होते थे तो उनकी माँ व्रत नहीं रखती थीं क्योंकि आर्य समाज के नियमों में व्रत प्रतिबंधित हैं। वेद प्रताप वैदिक ने भी आर्य समाज के नियमों का पालन किया लेकिन लड़कियों की आज़ादी को लेकर वे उदार थे। सहशिक्षा वाले विद्यालय में पढ़ी अपर्णा जी को बाहर आने जाने या लड़कों से ही दोस्ती करने जैसे प्रतिबन्ध का सामना नहीं करना पड़ा।
उनके घर के एक कमरे में उनके माता-पिता की किताबें भरी हुई थीं। अपर्णा जी बताती हैं “किताबों की रैक की उंचाई छत तक पहुँच गयी थी। साल में एक बार उन किताबों को निकालकर धूप दिखाई जाती, उन पर जिल्द चढ़ायी जाती। यह काम हम बच्चो के जिम्मे होता था।” जैसे ही बच्चे पढ़ने-लिखने लगे घर में उनके लिए भी पत्रिकाएँ आने लगीं। पराग, नंदन, चम्पक, चंदामामा और लोटपोट जैसी पत्रिकाओं की वजह से अपर्णा जी में पढ़ने की आदत बचपन में ही विकसित हो गयी। उनकी स्कूली शिक्षा सरदार पटेल विद्यालय से हुई जिसका संचालन गुजरात एजुकेशन सोसायटी करती थी। यहाँ छठवीं तक हिंदी माध्यम से ही पढ़ाई होती थी। अपने विद्यालय के बारे में अपर्णा बताती हैं, “मेरा स्कूल, कॉन्वेंट और सरकारी स्कूल दोनों के बीच था। पिताजी हिन्दी के बड़े समर्थक थे और उसे आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम कर रहे थे, इसलिए उनकी यह सोच थी कि बच्चों को हिन्दी भाषा की समझ तो होनी ही चाहिए।” वर्ष 1993 में हायर सेकेंडरी करने के बाद उनका दाखिला सेंट स्टीफेंस कॉलेज में हुआ, वहाँ से इतिहास विषय लेकर 1996 में स्नातक करने के बाद वे स्नातकोत्तर की उपाधि के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड चली गयीं। वर्ष 1999 में स्नातकोत्तर करने के बाद वे भारत लौटीं और जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय से पीएचडी के लिए अपना पंजीयन करवाया ।
कैम्ब्रिज जाने से पहले की घटना है, अपर्णा कुछ पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगी थीं। जैसे संपादक के नाम पत्र, यात्रा आधारित पत्रिकाओं में लेख या कुछ रोचक लेख आदि। सुविख्यात पत्रकार एच.के. दुआ के पुत्र सेंट स्टीफेंस कॉलेज में उनके साथ पढ़ते थे। अपर्णा कहती हैं, “मेरा छोटा-मोटा पोर्टफोलियो तैयार हो गया था, जिसे लेकर मैं दुआ अंकल के पास चली गयी। मैंने अपनी फाइल पकड़ा दी और दुआ अंकल ने उसे थोडा सा उलट पुलटकर देखा और फाइल बंद कर दी। फिर उन्होंने कहा -बेटा, अभी पढ़ाई कर रही हो, तो अभी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं चुपचाप वापस आ गयी और इसके बाद फिर पत्रकार बनने के बारे में सोचा भी नहीं।”
इस तरह उन्होंने मन ही मन यह तय कर लिया था कि अब अकादमिक क्षेत्र में ही जाना है। लंदन में खुद को लेकर, अपने समाज को लेकर यहाँ तक कि अपने देश को लेकर उनकी उनकी समझ कुछ और विस्तृत हुई। वे कहती हैं, “भारतीय होने का अर्थ देश से बाहर जाकर ही पता चलता है। अपने देश में तो सभी भारतीय हैं। मैं आज से बीस साल पहले लन्दन गयी थी। हो सकता है आज सोच बदल गयी हो लेकिन उस समय पूर्व में गुलाम रहे देश को लेकर उनकी सोच साफ़ पता चल रहा था।”
वर्ष 2000 में पीएचडी के लिए पंजीयन करवाने के एक साल के बाद उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में सहपाठी रहे श्री अनिल सांवरिया को अपना जीवन साथी बना लिया। उस वक़्त हालाँकि दोनों की उम्र कम थी और आर्थिक रूप से गृहस्थी शुरू करने की स्थिति में नहीं थे। अनिल जी बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलते थे लेकिन घर बसाने के लिए वे अपने भाई के व्यवसाय के साथ जुड़ गये। वर्तमान में वे क्रिकेट के प्रशिक्षक हैं। इधर अपर्णा जी अलग-अलग कॉलेजों में अतिथि व्याख्याता के रूप में पढ़ाने लगीं। यह सिलसिला 2005 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इतिहास पर केंद्रित उनकी पीएचडी पूरी होने तक चलता रहा।
वे कहती हैं, “अंडमान को लेकर हमारे बीच एकमात्र सोच यह है कि वहां क्रांतिकारियों को बंद रखा जाता था, यातनाएं दी जाती थीं जबकि यह सब अंडमान के इतिहास का छोटा सा हिस्सा भर है। शुरुआत में वहां कैदियों को ले जाकर सिर्फ जंगल साफ़ करवाया जाता था। लगभग पचास साल के बाद जेल की ईमारत बनी। उस ईमारत में कैदियों को ले जाने के बाद कुछ महीने रखते थे फिर उन्हें बस्तियों में छोड़ दिया जाता था लेकिन क्रांतिकारियों को जेल में ही बंद रखा जाता था।"
वर्ष 2007 में उन्हें अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में बतौर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर उन्हें नियुक्ति मिल गयी और वे अमेरिका चली गयीं। अनिल जी जो अपने भाई के साथ व्यवसाय कर रहे थे, वे बीच बीच में आते-जाते रहते थे। तब तक अमेरिका में 9/11 की भयावह घटना हो चुकी थी। हिंसा को लेकर वहाँ के अकादमिक क्षेत्र में खूब चर्चा और शोधकार्य हो रहे थे। अपर्णा जी के अनुसार लंदन और अमेरिका में एक फर्क है। लंदन में भारतीयों को उस औपनिवेशिक देश के नागरिक के तौर पर देखा जाता था जिस पर उन्होंने शासन किया जबकि अमेरिका की समस्या रंगभेद थी। भारतीयों को लेकर अमेरिकी नागरिकों की सोच वैसी नहीं थी जैसी लन्दन में देखने को मिली। इसके अलावा रेखांकित करने योग्य बात वे यह कहती हैं कि ‘अमेरिका के रंगभेद की समस्या से मुझे अपने देश के जातिवाद को समझने में मदद मिली।” वहां लेबनान और जॉर्डन जैसे मध्य एशिया के भी कई लोग थे। वहाँ हो रही चर्चा और विकसित हुई समझ का अपर्णा जी के शोध कार्यों का आधार कहा जा सकता है।
इस बौद्धिक सफ़र के अलावा उनके निजी जीवन में भी कुछ बदलाव हुए। वे दो बच्चों की माँ बन गयीं, जिनके साथ अकेले रहते हुए नौकरी को निभाना कठिन होता जा रहा था। एक बार उनके बड़े बेटे की तबियत खराब हुई जिसे लेकर उनके पति अस्पताल में थे और अपने छोटे बेटे को लेकर वे घर में रहीं। आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मदद मिल सके इसलिए एक नैनी की व्यवस्था की गयी। जब वह बच्चे को संभालती तब तक वे कुछ घंटे सो पातीं। ऐसे कठिन समय में अपना घर, अपना देश और पीछे छूटे चचरे-ममेरे भाई-बहनों की याद उन्हें सताने लगी। फिर उन्होंने अपने देश लौटने का फैसला किया। सपरिवार लौटने के बाद एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं थी। आर्थिक समस्या के कारण वे कुछ समय बाद फिर अमेरिका चली गईं और 2014 में अशोका विश्विद्यालय में नियुक्ति होने पर वापस लौटीं। उन्होंने पाया कि इस दौरान उनके परिजन वैचारिक रूप से पूरी तरह बदल चुके थे। भीड़ द्वारा एक व्यक्ति को पीट-पीटकर मार डालने की घटना पर उन्होंने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप दुःख जताया तो परिवार के सदस्य उन पर हमलावर हो गये। इस घटना का पुरजोर समर्थन करते हुए उनके कुछ भाई एक सुर में उन्हें ‘वामी’ कहने लगे। इस दौरान जिस भाषा और शब्दावली का वे प्रयोग कर रहे थे, वह कोई भाई अपनी बहन के लिए नहीं करता। इस घटना से वे क्षुब्ध हो गयीं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि एक हिंसक घटना का विरोध करने से वे ‘वामपंथी’ कैसे हो गयीं।
वे कहती हैं, “मैं हैरान थीं, मेरा वामपंथी दलों या उनकी राजनीति से सीधा कोई वास्ता नहीं था। मेरे पिता जनसंघ से जुड़े हुए और हिन्दूवादी थे ये सभी जानते हैं, लेकिन उन्होंने भी कभी इस तरह के विचारों का समर्थन नहीं किया। किसी और धर्म से नफ़रत करना जरुरी है यह उन्होंने कभी नहीं बताया। तो यह ज़हर आया कहाँ से और इसकी गहराई कहाँ तक है?” इस घटना ने और अमेरिका के अनुभवों ने मिलाजुलाकर एक पुस्तक की पृष्ठभूमि तैयार की जो 2020 में ‘My Son’s Inheritance: A Secret History of Lynchings and Blood Justice in India’ के नाम से आयी। इस पुस्तक में सामाजिक हिंसा के इतिहास को लेकर व्यापक पड़ताल दर्ज है। इससे पहले उनकी अंडमान द्वीप समूह के इतिहास पर पुस्तक प्रकाशित हो चुकी थी। इसके बाद उन्हें भी नहीं पता कि किस तरह उन्हें वामपंथी करार दे दिया गया और उनके लिखे-कहे का अर्थ तोड़-मरोड़कर उन्हें निशाना बनाया जाने लगा।
जब वे अमेरिका में पढ़ा रही थीं उस समय हिंसा को लेकर हो रही चर्चा की वजह से उन्होंने अपने देश के इतिहास और समाज को शोध का विषय बनाया। भारत के क्रांतिकारियों पर उनकी अब तक दो पुस्तकें आ चुकी हैं| एक पुस्तक में उन्होंने क्रांतिकारियों के अन्तः जीवन पर प्रकाश डाला है। यानि आन्दोलन से जुड़े हुए क्रांतिकारी किस तरह का जीवन जीते थे। अपने निजी जीवन में वे कैसे थे? अपर्णा जी कहती हैं, “वे बिलकुल हमारी आपकी तरह के इंसान थे। आम युवा की तरह ही खिलंदर और मस्त मौला। वे हर वो काम करते थे जो आम युवा करता है। पर साथ ही शहादत के लिए तत्पर आज़ादी की दीवाने भी थे।” शोधकार्य आगे बढ़ा और 20 24 में उनकी किताब आई - Revolutionaries of Trial: Sedition, Betrayal and Martyrdom.
यह पुस्तक लाहौर षड्यंत्र मामले और इसके प्रमुख शहीदों - भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु; और उनके कई सहयोगियों पर चलाए गए मुकदमों का एक अभूतपूर्व अध्ययन है। भारतीय, पाकिस्तानी और ब्रिटिश अभिलेखागारों से प्राप्त दुर्लभ और अनछुए सन्दर्भों पर आधारित यह पुस्तक लाहौर मुकदमे की कहानी को अलग तरफ से प्रस्तुत करती है। इसमें कई सवाल भी उठाए गए हैं जैसे - जब औपनिवेशिक राज्य के पास हिंसा और दमन का विकल्प मौजूद था तो उन्होंने मुकदमा चलाने की जहमत क्यों उठाई? क्या वह मुकदमा उनकी रणनीति थी जिसके माध्यम से वे अंग्रेजी शासन को न्याय का पक्षधर साबित करना चाहते थे? दूसरी तरफ ट्रायल के दौरान क्रांतिकारियों की रणनीति क्या रही? मुकदमे ने क्रांतिकारियों के बारे में जनता की धारणा को किस तरह से बदला? यह पुस्तक अभियुक्त के रूप में औपनिवेशिक राज्य, प्रतिवादी के रूप में क्रांतिकारी, अभियोजन पक्ष के गवाहों के रूप में गद्दार और दर्शकों के रूप में भारतीय प्रेस और जनता की पड़ताल करती है।
इस पुस्तक पर 2024 के दिसंबर में आयोजित कानपुर पुस्तक मेले में चर्चा हुई जिसमें अपर्णा और एक साक्षात्कारकर्ता मौजूद थे। चर्चा शानदार रही, अपर्णा से बातचीत कर रहे साक्षातकर्ता एक शब्द को हिन्दी में ठीक से नहीं बोल सके। वहां मौजूद श्रोताओं ने उस पर आपत्ति दर्ज की जिसका अपर्णा जी ने भी समर्थन किया। बात आई गई हो गयी लेकिन कुछ ही समय बाद यह प्रकरण एक आरोप के रूप में सामने आया। अपर्णा जी को ट्रोल करने वालों की जमात खड़ी हो गई और यह विवाद उनके स्पष्टीकरण के बावजूद नहीं थमा। वे दुःख जताते हुए कहती हैं, “लोग अपनी राय देने से पहले पढ़ते क्यों नहीं हैं?” अपनी विचारधारा को लेकर वे कहती हैं, “जिस माहौल में मेरी परवरिश हुई, वहां अलग विचार रखने की पूरी जगह होती थी भले ही वे मेरे माता-पिता से अलग हों। मैं ऐसा ही माहौल अब अपने बच्चों को देना चाहती हूँ|”
वर्तमान में वे अशोका विश्वविद्यालय, सोनीपत में व्याख्याता हैं और दिल्ली में अपने परिवार के साथ निवास कर रही हैं। अब तक विभिन्न शोध पत्रिकाओं में अपर्णा जी के सैकड़ों शोधपत्र प्रकाशित हो चुके हैं। ऐतिहासिक विषयों पर आधारित कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों में वे सम्मिलित हो चुकी हैं। इसके अलावा उन्हें कई राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है।
प्रकाशित कृतियाँ
• Revolutionaries of Trial: Sedition, Betrayal and Martyrdom, Aleph, India-2024
• Waiting for Swaraj: Inner Lives of Indian Revolutionaries, Cambridge University Press-2021
• My Son’s Inheritance: A Secret History of Lynchings and Blood Justice in India, Aleph, India-2020
• Imperial Andamans: Colonial Encounter and Island History Palgrave MacMillan, UK-2010
पुरस्कार/ सम्मान
• वर्ष 1999 में इतिहास विषय में उत्कृष्ट योगदान हेतु कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा डोरोथी फोस्टर स्टर्मन पुरस्कार
• वर्ष 1999 में वरिष्ठ शोध प्रबंध हेतु कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा बेसिल चैम्पनेस पुरस्कार
• वर्ष 1997 में विश्वविद्यालय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय, भारत द्वारा दीप चंद स्मृति पुरस्कार
• वर्ष 1996 में उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन हेतु सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली द्वारा वेस्टकोट स्मृति पुरस्कार
• वर्ष 1996 में इतिहास विषय में उत्कृष्ट योगदान हेतु सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली द्वारा ई. आर. कपाड़िया स्मृति पुरस्कार
• वर्ष 1995 में विश्वविद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए, सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली द्वारा शंकर प्रसाद स्मृति स्वर्ण पदक
प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अनुदान
• 2021 : यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के ग्लोबल इंगेजमेंट ऑफिस द्वारा ‘एंटी-कास्ट हायर एजुकेशन प्रोग्राम’ विकसित करने हेतु £4000 का अनुदान
• 2020 : ब्रिटिश अकादमी, सार्वजनिक इतिहास परियोजना के लिए £50,000 का शोध अनुदान
• 2019 : विट्स विश्वविद्यालय, द. अफ्रीका द्वारा एंड्रयू मेलन गवर्निंग इंटिमेसीज़ प्रोजेक्ट के लिए $19,000 का अनुदान
अन्य अंतर्राष्ट्रीय शोध अनुदान
• 2013: कॉम्पिटेटिव रिसर्च ग्रांट , जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय, यू.एस.ए.
• 2012: समर रिसर्च ग्रांट, जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय, यू.एस.ए.
• 2010: समर रिसर्च ग्रांट, जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय, यू.एस.ए.
• 2008: समर रिसर्च ग्रांट, जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय, यू.एस.ए.
• 2006: डॉक्टरेट हेतु पूर्व शोध के लिए अध्ययन अनुदान, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, भारत
• 2005: इंग्लैंड में शोध के लिए अध्ययन अनुदान, चार्ल्स वॉलेस इंडिया ट्रस्ट, यू.के.
• 2004: पीएचडी क्षेत्र कार्य के लिए अध्ययन/यात्रा अनुदान, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, भारत
शोध फैलोशिप
• 2014: लाल बहादुर शास्त्री अकादमी, मसूरी, भारत से वरिष्ठ फैलोशिप की पेशकश हुई थी, जिसे अशोका विश्वविद्यालय में नौकरी मिल जाने के कारण अपर्णा जी ने स्वीकार नहीं किया ।
• 2002: भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, भारत से जूनियर रिसर्च फैलोशिप प्राप्त हुई।
सन्दर्भ स्रोत : अपर्णा वैदिक से सारिका ठाकुर की बातचीत पर आधारित
© मीडियाटिक





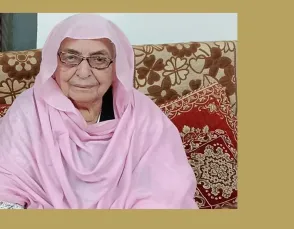




Comments
Leave A reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *